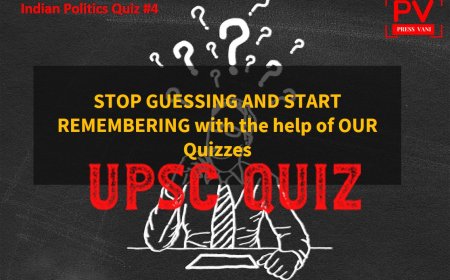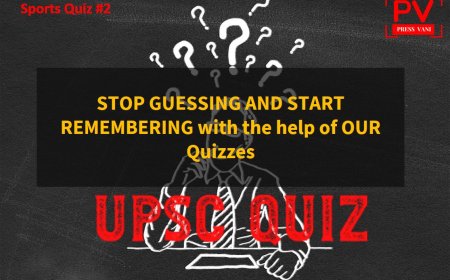Health & Lifestyle
Center Swung Into Action After Indian Spice Brands Banned In Hong Kong, Singapore
Pressvani Apr 22, 2024 0 24